वैश्विक स्तर पर इस समय सबसे अधिक चर्चा का विषय है जलवायु संकट (Climate Crisis) और इसके कारण होने वाली चरम मौसमी घटनाएँ। संयुक्त राष्ट्र (UN) और विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों की हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पृथ्वी का औसत तापमान पिछले एक दशक में अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, और बाढ़, सूखा, और तूफानों जैसी प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि देखी जा रही है। यह संकट अब केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक स्तर पर भी वैश्विक समुदाय को प्रभावित कर रहा है। इस लेख में हम इस संकट के विभिन्न पहलुओं, इसके कारणों, प्रभावों, और संभावित समाधानों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
जलवायु संकट का वर्तमान परिदृश्य
संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की नवीनतम रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि तत्काल और ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो वैश्विक तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पार कर सकती है, जो पेरिस समझौते का प्रमुख लक्ष्य है। 2025 तक, कई क्षेत्रों में पहले से ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, असामान्य बारिश, और चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि देखी जा रही है। उदाहरण के लिए, इस वर्ष यूरोप में अभूतपूर्व गर्मी की लहरों ने हजारों लोगों की जान ली, जबकि दक्षिण एशिया में मॉनसून की अनियमितता ने भारत, बांग्लादेश, और पाकिस्तान में भयावह बाढ़ का कारण बना।
संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव आमिना मोहम्मद ने हाल ही में ताजिकिस्तान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन में कहा, “जल-सम्बन्धी पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।” हिमनदों का तेजी से पिघलना न केवल जलवायु संकट का एक लक्षण है, बल्कि यह उन लाखों लोगों के लिए खतरा है जो अपनी जल आपूर्ति के लिए इन पर निर्भर हैं।
Business Loan
Get personal loan up to 5 CR
Home Loan
Get home loan up to 50 lakhs
जलवायु संकट के प्रमुख कारण
जलवायु संकट के लिए मानव गतिविधियाँ मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। इनमें शामिल हैं:
-
जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग: कोयला, तेल, और प्राकृतिक गैस के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) और अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जो वायुमंडल में गर्मी को फँसाती हैं।
-
वनों की कटाई: जंगलों को काटने से न केवल CO2 को अवशोषित करने की पृथ्वी की क्षमता कम होती है, बल्कि यह जैव विविधता के लिए भी खतरा है। अमेज़न और इंडोनेशिया के वर्षावनों में हाल के वर्षों में वनों की कटाई में तेजी आई है।
-
औद्योगिक और कृषि उत्सर्जन: मीथेन (CH4), जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, पशुपालन और धान की खेती से निकलता है। इसके अलावा, रासायनिक उर्वरकों और औद्योगिक प्रक्रियाओं से नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) का उत्सर्जन भी बढ़ा है।
-
उपभोक्ता संस्कृति: तेजी से बढ़ती उपभोक्ता मांगों ने उत्पादन और परिवहन की प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया है, जिससे ऊर्जा की खपत और उत्सर्जन में वृद्धि हुई है।
वैश्विक प्रभाव और चुनौतियाँ
जलवायु संकट के प्रभाव अब हर महाद्वीप पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं:
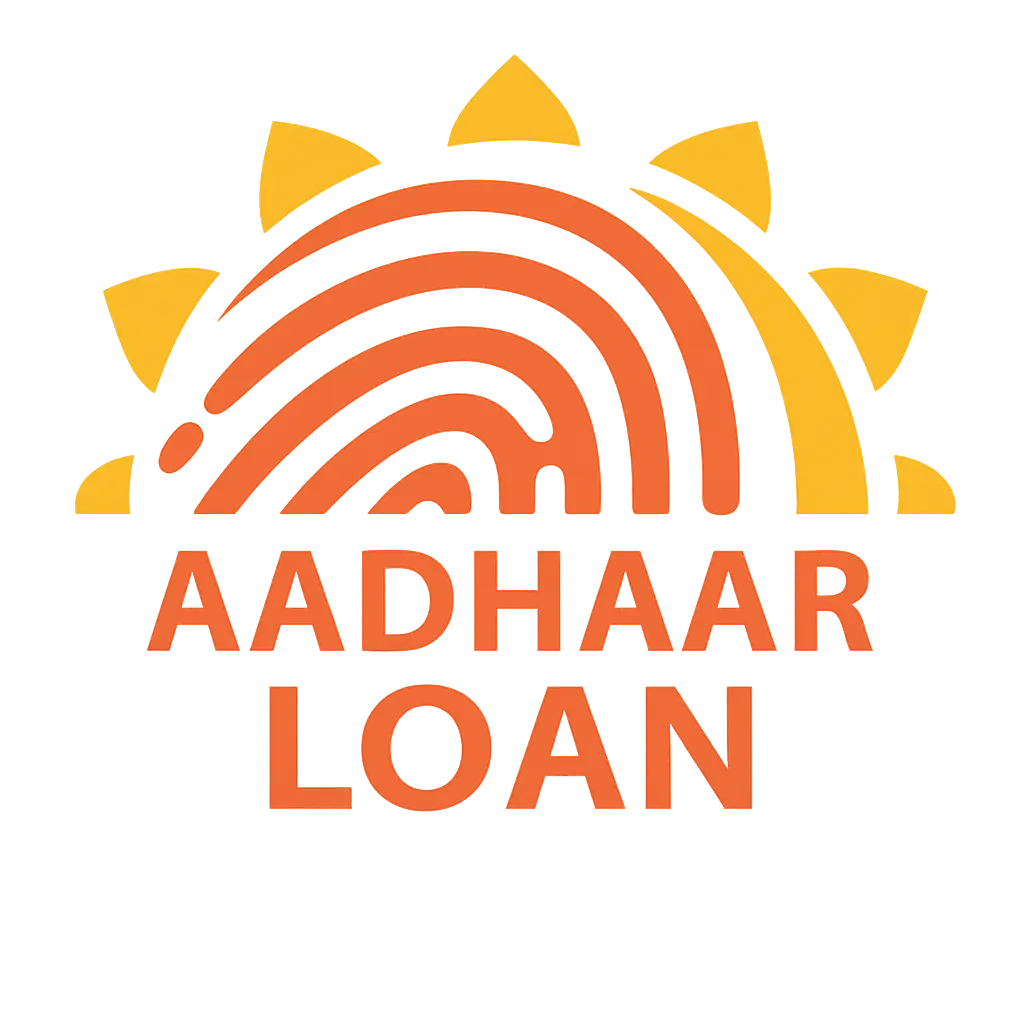
Aadhar Pe Loan
Get aadhar loan up to 1 lakhs
Personal Loan
Get personal loan up to 5 lakhs
-
चरम मौसमी घटनाएँ: 2025 में ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया में जंगल की आग ने लाखों हेक्टेयर भूमि को नष्ट कर दिया, जबकि भारत और अफ्रीकी देशों में बाढ़ और सूखे ने फसलों को भारी नुकसान पहुँचाया।
-
समुद्र स्तर में वृद्धि: ग्लेशियरों और ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय शहर जैसे मियामी, मुंबई, और ढाका खतरे में हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, 2050 तक 30 करोड़ लोग समुद्र स्तर वृद्धि से प्रभावित हो सकते हैं।
-
जैव विविधता का ह्रास: जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवाल भित्तियाँ (Coral Reefs) मर रही हैं, और कई प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पर हैं। ग्रेट बैरियर रीफ का लगभग 50% हिस्सा पहले ही नष्ट हो चुका है।
-
आर्थिक नुकसान: विश्व बैंक के अनुसार, जलवायु परिवर्तन से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2030 तक 18% तक की हानि हो सकती है। विकासशील देश, जो उत्सर्जन में कम योगदान देते हैं, सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।
-
स्वास्थ्य संकट: गर्मी की लहरें, वायु प्रदूषण, और जलवायु परिवर्तन से फैलने वाली बीमारियाँ (जैसे डेंगू और मलेरिया) वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव डाल रही हैं।
वैश्विक प्रतिक्रिया और प्रयास
जलवायु संकट से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय कई स्तरों पर प्रयास कर रहा है। कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:
-
पेरिस समझौता: 2015 में हस्ताक्षरित इस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। हालांकि, कई देश अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने में पीछे हैं।
-
नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश: सौर और पवन ऊर्जा में निवेश बढ़ रहा है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जबकि यूरोपीय संघ 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बना रहा है।
-
कार्बन प्राइसिंग: कुछ देश कार्बन उत्सर्जन पर कर लगा रहे हैं, ताकि कंपनियों को स्वच्छ ऊर्जा की ओर प्रोत्साहित किया जा सके।
-
जलवायु वित्त: विकसित देशों ने विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए 100 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष प्रदान करने का वादा किया है, हालांकि इस लक्ष्य को पूरा करने में देरी हो रही है।
-
युवा आंदोलन: ग्रेटा थनबर्ग जैसे युवा कार्यकर्ताओं ने जलवायु कार्रवाई के लिए वैश्विक आंदोलनों को प्रेरित किया है। 2025 में, लाखों युवा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
भारत का योगदान और चुनौतियाँ
भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है, जलवायु संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है और नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी से प्रगति कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की पूर्वोत्तर भारत जैव-सांस्कृतिक पहल (NEBI) के तहत, आदिवासी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके हरित समाधानों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
हालांकि, भारत के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। कोयले पर निर्भरता, शहरीकरण, और बढ़ती ऊर्जा माँग के कारण उत्सर्जन को कम करना कठिन है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे बाढ़, सूखा, और गर्मी की लहरें भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहे हैं।
समाधान और भविष्य की दिशा
जलवायु संकट से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं:
-
उत्सर्जन में कटौती: सभी देशों को अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को सख्त करना होगा और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करनी होगी।
-
जंगल संरक्षण: वनों की कटाई को रोकना और पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है।
-
सतत विकास: हरित प्रौद्योगिकियों और सतत कृषि प्रथाओं को अपनाने से उत्सर्जन कम हो सकता है।
-
वैश्विक सहयोग: जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से विकासशील देशों का समर्थन करना जरूरी है।
-
जागरूकता और शिक्षा: लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और समाधानों के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है।
निष्कर्ष
जलवायु संकट आज की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है, जिसका समाधान केवल सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। यह न केवल पर्यावरणीय, बल्कि मानवीय और आर्थिक संकट भी है। यदि हम अभी कार्रवाई नहीं करते, तो आने वाली पीढ़ियों को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वैश्विक समुदाय, सरकारें, और नागरिकों को मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरश ने कहा, “हमारे पास अभी भी समय है, लेकिन यह तेजी से खत्म हो रहा है।” यह समय है कि हम अपने ग्रह को बचाने के लिए एकजुट हों।












